|
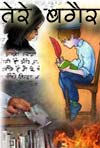
सुख है कि
उनके जाने का यकीन नहीं
वे हँसती थीं तो किसी को
यकीं ही नहीं होता था कि उनके जीवन में दुःख का कोई साया
भी पड़ा होगा। चमकते दाँत‚ नीली व भूरी कंचई आँखें‚ मुझे अब
भी याद है। उनकी सुंदरता और विद्वता की चर्चा मैंने एक साथ
सुनी और देखी थी। इसलिए जब मुझे पता चला था कि उन्हें
कैंसर है और इलाज के बाद तमाम अस्पतालों में कोशिश के बाद
थक हार कर जब उन्हें फिर उनके पिता के घर कोलकाता लाए जाने
की खबर मिली‚ तो भी मैं उनके यहाँ जाने का साहस नहीं जुटा
पाया। इसलिए अंतिम यातनास्पद हालातों से मैं अछूता ही रहा।
जो मेरे लिए कम यातनास्पद अब नहीं रह गया है। एक मरते हुए
व्यक्ति से मिलने से पलायन मुझे जब तब सालता रहता है।
डॉक्टर इलारानी सिंह ने डबल डीलिट किया था। कोलकाता के
जयपुरिया कालेज में रीडर थीं। कोलकाता विश्वविद्यालय में
मेरे पीएचडी की गाइड । लेकिन इतना भर ही तो नहीं था। वे
स्वयं कवि और आलोचक थीं। उनकी कविताओं की पुस्तक 'वात्या’
पर मैंने अपने जीवन की पहली समीक्षा लिखी थी। लेखन को लेकर
उनसे लगातार फटकार सुनना रहा‚ प्रशंसा कम। वे चलताऊ लेखन
को कभी पसंद नहीं करती थीं। अखबारी लेखन उनकी दृष्टि में
हमेशा ही हीन रहा। वे निरंतर शाश्वत मुद्दों और
चुनौतीपूर्ण लेखन के लिए न सिर्फ प्रेरित करती रहीं‚बल्कि
अपने लिए भी उन्होंने यही रास्ता चुना था। शिलाखंड
'राउलवेल’ पर लिखी इबारतों पर उनका विश्लेषणात्मक ग्रंथ इस
बात का प्रमाण है कि वे किस तरह के गंभीर व चुनौती पूर्ण
विषयों से जूझती रही थीं।
'कवि मुक्तिबोध’ पुस्तक कंपोज हो रही थी‚ उन्हीं दिनों में
उनके संपर्क में आया था। अपने लिखे को भी बार–बार वे इस
लिहाज से देखती थीं कि संशोधन की गुंजाइश तो नहीं? 'अँधेरे
में’ कविता की व्याख्या लिखने के बाद भी उसमें और पुख्तापन
लाने के लिए कविता का सैकड़ों बार पाठ करते मैंने उन्हें
देखा। वे लगातार अपने लिखे में एक नई कौंध का इंतजार करते
हुए दिखी थीं। लिखना उनके लिए एक बेचैनी से गुजरना ही था।
कविताएं लिखते समय तो उन्हें एकदम एकांत चाहिए होता था।
मेरी तरह नहीं कि भीड़ भरी ट्रेन में लिख मारा। और कहीं
नहीं जगह मिली और मूड जम गया तो रेलवे स्टेशन की की गंदी
सीढ़ियों पर अखबार बिछा कर बैठ गए और लिख लिया‚ वरना लिखा
टल गया तो फिर गया। सियालदेह स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठ
मैंने कितनी ही कविताओं को लिखा है।
टीटागढ़ से लोकल ट्रेन पकड़ सियालदह आने के क्रम में अक्सर
इतनी भीड़ का सामना करना पड़ता कि कई बार साँस लेने के लिए
भी गुंजाइश निकालनी पड़ती। चारों तरफ से लोगों के बीच दबे
हुए अक्सर मन कहीं और दौड़ाना‚ किन्हीं स्मृतियों में अपने
को डुबो देने का निरंतर प्रयास मैं करता जिससे की उस कष्ट
को मैं भूल सकूँ। और इसी क्रम में कई रचनाएँ उपजीं। लेकिन
यह गुंजाइश कतई नहीं होती थी कि मैं अपना हाथ अपनी जेब तक
ले जाकर पेन निकाल सकूँ। कागज पर कुछ लिख पाने की तो खैर
कल्पना तक व्यर्थ थी। सो जैसे ही सियालदह ट्रेन से उतरता
उस व्यस्ततम स्टेशन पर कहीं बैठने की जगह मिलना लगभग
नामुमकिन होता था सो स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर ट्रेन में
सोचे गए को याद कर लिखने की कोशिश मैं करता कई बार सफल भी
हो जाता। कई बार बात जेहन से निकल जाती या अधूरी ही याद
पड़ती।
धीरे-धीरे मैं अपनी रचनाओं के कारण ही उनके करीब होता गया।
अक्सर उनके घर आना-जाना होता। उनकी पारिवारिक जिंदगी से भी
वाकिफ होता चला गया। उनके पति भागलपुर विश्वविद्यालय में
मैथिली के रीडर हैं। कोलकाता के जालान गर्ल्स कॉलेज में
शादी के पहले पढ़ाती थीं। शादी के बाद पति के साथ रहने के
उपक्रम में वे भागलपुर चली गईं। विभागों के .फर्क के
बावजूद एक ही जगह अध्यापन शुरू किया था। मगर दोनों की अनबन
ऐसी हुई कि वे अपने पिता के यहाँ कोलकाता लौट आई थीं। साथ
उनकी संतानें दो बेटे और एक बेटी भी थी। उन दिनों एक
दिल्ली में पढ़ रहा था‚ एक सिंधिया कॉलेज‚ ग्वालियर में।
बेटी थी साथ। बाद में पति उन्हें वापस लेने भी आए थे मगर
वे स्वाभिमान व जिद में फिर नहीं लौटीं। तलाक भी नहीं
दिया।
उनकी बंगाली सौतेली माँ डॉक्टर अणिमा सिंह लेडी ब्रेबार्न
कालेज प्रोफेसर तथा पिता डॉक्टर प्रबोध नारायण सिंह
कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनके घर पर
हिन्दी‚ मैथिली और बांग्ला विद्वानों का जमघट ही लगा रहता
था। मुझे वहाँ चाहे–अनचाहे बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस
चित्रकार गणेश पाइन को मैं ग्रेस सिनेमा के पीछे एक
चायखाने विभूति केबिन में दूर-दूर से देखा करता था‚ उनसे
मेरा प्रत्यक्ष परिचय कराया था। बाद में तो मैं अक्सर उनकी
अड्डेबाजियों में शामिल हो गया था। जहाँ युवा चित्रकार
विमल कुंडू भी आता था बाकी कवि आलोचक ही थे। और जहाँ मैंने
उन लोगों का बाँग्ला साहित्य‚ कला और फिल्मों में
उत्तर–आधुनिकता के आंदोलन का स्वरूप निर्धारित करते हुए
पाया। हिन्दी में तो बाद में सुधीश पचौरी आदि के लेखों में
उत्तर आधुनिकता की चर्चा पढ़ने में आई थी। गणेश पाइन ने ही
इला जी की 'कवि मुक्तिबोध’ पुस्तक का आवरण चित्र बनाया था।
और मेरी पहली पुस्तक का कवर बनाने का वादा भी किया था।
चूँकि उनके यहाँ मैथिली‚ बाँग्ला और अंग्रेजी तीनों बोली
जाती थीं सो थोड़ी बहुत मैथिली मैंने भी सहज ही सीख ली तो
कोई हैरत नहीं। इला जी ने सागर विश्वविद्यालय से एम॰ ए॰
किया था‚ जहाँ उन्होंने आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी‚ डॉक्टर
शिवकुमार मिश्र जैसों से रचना दृष्टि पाई थी और बाद में
अपने गुरुओं की स्नेह-भाजन रहीं। संभवतः दो भिन्न दिशाओं
के गुरुओं के कारण ही उनके रचना-संस्कार में प्रगतिशीलता
और परंपरावाद का मिश्रण मिलता है। उन्होंने जो कुछ मुझे
दिया वह ये कि किसी से आक्रांत न होने का माद्दा। चुनौती
को स्वीकार करने की आदत‚ जिसकी तो वे प्रतिमूर्ति ही थीं।
लिखने में लापरवाही के लिए सुनी फटकारों के बाद मुझे
बाकायदा रोते हुए उनके घर वालों ने भी देखा और मेरे साथ
उनके निर्देशन में काम करने वाले अन्य शोधार्थियों ने भी।
आखिर कभी न कभी उनकी भी बारी आई ही। अच्छे मूड में हों तो
वे जितनी मीठी थीं‚ नाराज होने पर उतनी ही कटु। लापरवाही
की वजह से मेरे हिस्से उनकी फटकारें बहुत आई थीं। एक ओर
भाषा विज्ञान और भाषा पर उनका आधिकारिक ज्ञान था। दूसरी ओर
साड़ियों‚ चूड़ियों साज श्रृंगार की चीजों के प्रति
स्त्रीयोचित ललक। खाने की बेहद शौकीन।
हर रविवार को बड़ाबाजार थाने के पास स्थित हनुमान मंदिर
टेंपल स्ट्रीट पुस्तकालय में वे तथा कई और कॉलेजों के
प्राध्यापक आकर निःशुल्क हिन्दी की शिक्षा देते थे। वहीं
वे तथा उनके पिता डॉक्टर प्रबोध नारायण सिंह अपने
शोधछात्रों का भी मार्गदर्शन करते थे। वहाँ साहित्यिक
कार्यक्रमों का आयोजन भी‚ उनकी प्रेरणा व प्रयास से होते
रहते थे। उन्हीं के कहने पर मैं जनवादी लेखक संघ से भी
जुड़ा‚ वरना साहित्य और कला जैसे विषयों में संघबद्धता पर
मेरा बहुत यकीन आज भी नहीं है। यह बात दीगर है कि एक वर्ष
बाद ही जनवादी लेखक संघ ने मेरा वार्षिक चंदा ५ रुपए
स्वीकार नहीं किया अर्थात मैं जलेस द्वारा खारिज कर दिया
गया था। हालाँकि बाद में जलेस के कई कार्यक्रमों में मुझे
रचनापाठ के लिए न्योता गया। और माकपा के साप्ताहिक मुखपत्र
'स्वाधीनता’ के शारदीय विशेषांक में दो बार कविताएँ भी
प्रकाशित हुईं। जहाँ काव्य–पाठ के दौरान बिना दूध की काली
चाय मिलती।
मेरे लिए शुरू शुरू में यह माहौल अजीब सा लगता था। मैंने
जिस माहौल में होश सँभाला था वहाँ कवियों के लिए भी साधारण
चमक–दमक थी। आठवीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था‚ गोंदिया अखिल
भारतीय कवि-सम्मेलन में मैंने काव्य–पाठ किया था। मैंने
हाफ पैंट पहन रखी थी। और उस समय मुझे १५ रुपए पारिश्रमिक
भी मिला था। तो जब मैं जनवादियों के संपर्क में आया तो
मुझे पता चला तमाम विख्यात साहित्यकारों की सभाओं में भी
प्रायः माइक नहीं होता और ना ही प्रकाश की समुचित व्यवस्था
थी। किसी भग्नप्राय स्कूल के कमरे में कार्यक्रम आयोजित
होता जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से राज्य सभा
की सदस्या सरला माहेश्वरी और चंद्रा पांडेय भी होतीं और
आलोचक डॉ. शंभुनाथ‚ कोलकाता में राजेंद्र यादव के जिगरी
दोस्त रहे अवधनारायण सिंह‚ प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर
डॉ. सुब्रत लाहिड़ी‚ विमल वर्मा‚ धुव्रदेव मि॰ पाषाण और
इसराइल भी। वे सकलदीप सिंह भी‚ जो हमेशा इस बात का विरोध
करते कि लेखकों पर पार्टी अपने निर्देश न थोपे। साहित्य को
कामरेड दिशा निर्देश करेंगे तो इससे साहित्य का अहित होगा।
केवल 'लाल सलाम’ लिखने से कोई अच्छा प्रतिबद्ध लेखक नहीं
हो सकता। उन दिनों पाषाण और श्रीहर्ष की कविताओं में 'लाल
सलाम’ कहीं न कहीं से जरूर आ जाता। यहीं पहली बार उन
शब्दों से परिचय हुआ‚ जो वर्गीय विभाजन से जुड़े हैं।
बुर्जुआ‚ सर्वहारा‚ दक्षिणपंथी जैसे शब्द इनके वक्तव्यों
में बार–बार आते। यहाँ बीड़ी पीते लेखकों की कमी न थी‚ जो
दूसरे की परवाह किए बिना पीते रहते। और कुछ ऐसे लोग भी
होते जो देसी शराब के नशे में धुत होते। मैं धीरे-धीरे इस
माहौल का अभ्यस्त हो गया।
वे सकलदीप सिंह मेरे दोस्त हो गए‚ जो कभी कम्युनिस्ट
पार्टी के कार्ड होल्डर थे। और बाद में पार्टी से इस्तीफा
दे दिया था। जो साठोत्तरी काव्यांदोलनों के समय श्मशानी
पीढ़ी का नेतृत्व करने वालों में से एक थे और जिन्हें निषेध
के कवि के तौर पर डॉ. जगदीश चतुर्वेदी ने अपने साथ शामिल
किया था।
वे इलाहाबाद विश्वविदयालय से अंग्रेजी तथा हिन्दी में एमए
करके कोलकाता आए थे। नेशनल लाइब्रेरी के नियमित पाठकों में
से एक। ७६ की उम्र में भी वे कोलकाता से अपने गाँव नहीं
लौट पा रहे हैं तो उसमें एक कारण किताबें भी हैं। वह छपरा
जिले के गाँव में कहाँ मिलेंगी। सकलदीप जी ने पाश्चात्य और
आधुनिक साहित्य का खूब मनन और अध्ययन किया है। और वे
नियमित लिख्खाड़ भी रहे हैं। मेरा खयाल है उनकी पचास
डायरियाँ उनकी कविताओं से भरी होंगी। एक बार जो लिख दिया
सो लिख दिया। उनकी कविता में कम से कम अपने द्वारा किया
गया संशोधन नहीं मिलेगा। अलबत्ता पुस्तक निकालते समय जरूर
अवध नारायण सिंह ने कहीं कुछ संशोधन किया होगा तो होगा।
उनके बाद दूसरा शख्स मैं बना काफी दिनों बाद जिसे उनकी
कविताओं में मनचाहे परिवर्तन की इजाजत थी। बाद में तो वे
कई लोगों से कहते भी सुने गए कि अभिज्ञात के बिना मैं
अधूरा महसूस करता हूँ।
वे कोलकाता छोड़ने के कुछ पहले कुछ मामलों में मुझ पर काफी
यकीन करने लगे थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनकी पुस्तक
पर भूमिका रहे। पर पहली बार ऐसा हुआ था। मैंने उनकी 'ईश्वर
को सिरजते हुए’ काव्य पुस्तक की भूमिका लिखी। अपनी एक
पुस्तक तो उन्होंने मुझे ही समर्पित की है। भूमिकाएँ लिखने
का अवसर मुझे कई बार हाथ लगा है। पहली बार रवींद्र कुमार
सिंह की पुस्तक 'सरकारी लाश’ की भूमिका मैंने लिखी थी। और
जिसे मैं अहम मानता हूँ वह है कीर्ति नारायण मिश्र की
'विराट वट वृक्ष के प्रतिवाद में’ की भूमिका। यों अमृतसर
में अमर उजाला में सहकर्मी और दोस्त हरिहर रघुवंशी के पहले
कहानी संग्रह की भूमिका भी मैंने लिखी। पर सबसे अवसाद भरी
भूमिका लिखनी पड़ी थी मुझे अमित राजोरिया की 'सरायखाना’ की।
सरायखाना १६-१७ वर्षीय उस अमित की कविताओं का संग्रह है जो
उसकी आकस्मिक मृत्यु के बाद छपी। अमित कपड़ा व्यापारी का
बेटा था‚ जो मेरे दोस्त थे। उनका साहित्य से कोई सरोकार
नहीं था। जब भी मैं उनके यहाँ जाता अमित मुझसे तरह तरह के
सवाल पूछता और एक दिन उसने बताया कि वह भी कविताएँ लिखता
है। उसकी दो एक पत्रिकाओं में कविताएँ अभी प्रकाशित ही हुई
थीं। बीमारी से उसकी आकस्मिक मौत के बाद उसके पिता प्रकाश
राजोरिया ने उसकी कविताओं की डायरी मुझे दी थी और कहा था
क्या इसे प्रकाशित किया जाना चाहिए। मैं यह देखकर रो पड़ा
था कि उसकी कविताओं की डायरी के कुछ सफे ऐेसे थे‚ जिसमें
एक तरफ मेरी कविताएँ उसने लिख रखी थीं दूसरी ओर अपनी। एकदम
आमने–सामने के पृष्ठों पर। मैं नहीं जानता कि मैं उसका
आदर्श था या प्रतिद्वंद्वी। पर मैं यह जानता हूँ कि कला के
क्षेत्र में जो हमारे आदर्श पुरष होते हैं‚ वही हमारे
प्रतिद्वंद्वी होते हैं। कितनी निष्ठुर होती है कला जगत की
सच्चाइयाँ कि हम जिसे चाहते हैं उसी को तोड़ते हैं। अपने
सबसे प्रिय की कलात्मकता को तोड़े बिना कोई कलाकार आगे नहीं
बढ़ सकता। अमित होता तो वह मुझे आज कहीं न कहीं नकारने की
तैयारी कर रहा होता। मुझे भी समय लगा है अपने प्रिय कवि
केदारनाथ सिंह के जादू से मुक्त होने में। और उनने भी अपने
काव्य गुरू त्रिलोचन से मुक्ति पाकर ही अपनी राह तलाश ली।
इला जी मुक्तिबोध को लेकर किताब लिखती रहीं। पर जब तक वह
किताब प्रकाशित होकर आती‚ मैं मुक्तिबोध के बारे में अपने
गुरू से स्वतंत्र राय कायम कर चुका था। शायद यह इला जी ही
थीं‚ जिनकी वजह से मैंने मुक्तिबोध की रचनाओं की करुणा से
परिचित हो सका।
इला जी से मिलकर मुझ में यह तो हुआ कि मैं साहित्य के
गंभीर सरोकारों से जुड़ा मगर पूरी तौर पर शाश्वतता के हवाले
अपने–आपको न कर सका। उसकी कुछ और वजहें भी थीं। मेरे
नानाजी केंद्र सरकार की जूट मिलों में ठेकेदार थे। उनके
काम में भी मुझे हाथ बँटाना पड़ता था। जो कि एक नीरस दुनिया
थी। साहित्य ही वह झरोखा था‚ जहाँ से मैं एक दूसरी दुनिया
में जा सकता था जो मुझे राहत देती। फिर मैं 'जनसत्ता’
अखबार से बतौर स्ट्रींगर जुड़ गया और समय कम पड़ने लगा।
अखबार से जुड़ना मेरी गुरू को कतई पसंद नहीं था। समय के
अभाव में मिलना-जुलना कम होने लगा। शोध का कार्य तो मेरा
चलता रहा था। पब्लिक सेमिनार में परीक्षकों में कई दिग्गज
थे। आचार्य विष्णुकांत शास्त्री भी थे‚ जो अब उत्तर प्रदेश
के राज्य पाल हैं। डॉ. चंद्रा पाण्डेय थीं जो माकपा की
राज्य सभा की सदस्य हैं। डॉ शंभुनाथ पीएचडी कमेटी के
कन्वेनर थे। चंद्रा जी ने उस सेमिनार में माना था कि शोध
में बेहद मौलिकता है। दूसरों के हवाले कम दिए गए हैं।
लेकिन इस तरह के काम को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है‚
क्योंकि यह परंपरागत शोध कारों से अधिक महत्व का है। अब
मुझे थीसिस जमा करनी थी।
इधर स्वयंभू भगवान बालक ब्रह्मचारी का निर्विकल्प समाधि
प्रकरण राज्य में चर्चा के केंद्र में था। उनकी मृत्यु के
बाद उनके शिष्य कह रहे थे कि उनके शव की अंतिम क्रिया नहीं
की जाएगी क्योंकि वे वापस लौटेंगे। वे भगवान हैं। उनका शव
५४ दिन तक सुरक्षित रखा गया था। जिसका सरकार ने अंततः जबरन
अंतिम संस्कार किया। इसकी कवरेज का जिम्मा मेरे ऊपर था। सो
मेरे पास अवकाश इतना नहीं था कि मैं शोध कार्य के लिए उनसे
मिलता। फिर भी किसी तरह पहुँचा तो पता चला कि गलतफहमियों
की एक दीवार हमारे बीच खड़ी हो चुकी थी।
किसी ने उनके कानभर दिए थे। उनका कहना था कि मैं तो किसी
और के अधीन शोधकार्य शुरू कर रहा हूँ। और यह भी कि मैं
कहता फिरता हूँ कि मैं उनसे बड़ा लेखक हूँ। वे मेरी बातें
सुनने को तैयार नहीं थीं। मैं रोते हुए लौट आया था। और
जबकि मेरी थीसिस जमा करने के कुल पाँच दिन बचे थे‚ बालक
ब्रह्मचारी की सड़ी हुई लाश निकालने के लिए पश्चिम बंगाल की
पुलिस ने व्यापक तैयारी के साथ आपरेशन सत्कार किया था। मैं
एक्सक्लूसिव कवरेज के चक्कर में पुलिस की लाठियों से बेतरह
जख्मी हो‚ हाथ पैर तुड़वाए डेढ़ महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा।
मगर उनकी ओर से समाचार नहीं पूछे जाने की यंत्रणा अधिक
दुखदायी रही। महीनों बाद फोन किया तो उनकी बेटी ने बताया
कि उन्हें कैंसर है। इलाज के लिए दिल्ली गई हैं। फिर फोन
किया तो पता चला घर वाले नाउम्मीद हैं। साहस जुटा रहा था
कि कैसे उनका सामना करूँ। अपनी नाराज गुरू से ऐसे मकाम पर
मिलने से मैं दो एक दिन कतराए रहा। इसी बीच उनके देहावसान
की सूचना मिली। मैं दुखी शर्मसार किस मुँह से उनके घर
जाता। उनके बडों और माँ बाप से मिलने।
मैंने जो अपराध किए ही नहीं उसकी सजा तो मैं काट ही रहा
था। जिनसे बहुत कुछ पाया‚ उनकी निगाह में ता-उम्र अपराधी
बना रहा। और अब तो यह गुनाह है ही कि उनके अंतिम दर्शन भी
नहीं किए। कहीं न कहीं मन में खौफ था मुझे– वे मुझे अपराधी
मानती ही हैं। जाने चला–चली की बेला में मुझे क्या कहें।
जिंन्दगी भर उनका कहा पीछा करेगा।
यह मेरा निहायत निजी सुख है कि मुझे उनके जाने का यकीन
नहीं होता। जब वे थीं‚ उनसे मेरी सुलह करवाने का वादा किया
था हृदयेश पांडेय ने‚ जो उनसे पहले ही दुनिया छोड़ गए। वे
अगर होते तो शायद वह नहीं होता जो मैं अभी हूँ। वे दक्षिण
भारत की हिन्दी फिल्मों में लिखते थे। कहानियाँ पटकथाएँ।
मेरे साथी बन गए थे। कवि सम्मेलनों में हम कई बार साथ रहे।
उन्होंने योजना बनाई थी साथ मिलकर लिखने की। जो अधूरी रह
गई।
जो सरलता है वह कितनी कठिन
'उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने यह सोचा, दुनिया को
हाथ की तरह मुलायम और गर्म होना चाहिए।’ यह वह कविता थी‚
जिसने मुझे बरबस अपने प्रति वीकनेस पैदा कर ली थी।
धीरे–धीरे मैं उनकी कविताओं में ऐसा डूबता गया कि मैंने
अपने पीएचडी का विषय ही केदारनाथ सिंह को बना डाला। उन
दिनों उनकी महज तीन ही काव्य पुस्तकें आई थीं। पुरस्कार
इक्के–दुक्के ही मिले थे। अकाडमी एवार्ड भी नहीं मिला था
तब तक। बाद में तो खैर हिन्दी में सर्वाधिक पुरस्कार
प्राप्त लेखकों में से वे हैं। केदार जी पर कार्य तो करता
रहा मगर‚ उनसे मिलने का अवसर बहुत बाद में मिला। एक विषय
भर थे‚ पहले वे मेरे लिए। एक अमूर्त व्यक्ति थे। एक रचना
की तरह। चूँकि उनका व्यक्तित्व भी मेरे विषय में शुमार था‚
सो उनके व्यक्तित्व को उनकी रचनाओं में पकड़ने की कोशिश
करना भी मेरे शोध के लिए अनिवार्य था। बाद में मिलना हुआ।
देर तक बातें भी हुईं। पहली बार तो तब जब वे हावड़ा में
अपनी बहन के यहाँ आए थे। उन्हीं से पता चला था चूँकि
दिल्ली में ठंड अधिक पड़ती है‚ सो जाड़े की शुरूआत में वे
उन्हें कोलकाता पहुँचा जाते हैं और जाड़ा बीत जाने पर फिर
दिल्ली अपने पास ले जाते हैं।
दीदी के ही घर पर मिला था पहले-पहल। पहले ही परिचय में
बहुत पुराने परिचित लगे। मुलाकात में कतई आक्रांत नहीं
करते। उनके मुँह से भोजपुरी सुनना भोजपुरी भाषा के निखार
को देखना लगा। काफी कुछ ललित निबंधकार डाक्टर कृष्ण बिहारी
मिश्र की तरह। भोजपुरी के बारे में उन्होंने अपने गुरू
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की चर्चा भी की। जयप्रकाश
नारायण का संस्मरण भी उन्होंने सुनाया था‚ जब वे पहले पहल
उनसे मिले थे।
फिर मुलाकात हुई तो पाया कि वे अस्वस्थ हैं। दीदी उनकी
छोटी बहन उनके तलवों में मालिश कर रही थी। वे लेटे हुए थे।
पता चला तेज ठंड वाली दिल्ली से माँ को बचाने और इधर बरसों
से दिल्ली ही रहने वाले केदार जी को कोलकाता की हल्की ठंड
रास नहीं आई थी। उस दिन वे लेटे-लेटे ही बात करते रहे।
बताया सुनील गंगोपाध्याय से मिलने गए थे। वहीं से अस्वस्थ
होकर लौटे हैं। उस दिन वे कोलकाता पर ही बतियाते रहे क़ि
गालिब अगर कोलकाता नहीं आते तो उनकी रचनाओं में जो पीड़ा है
यथार्थ है‚ वह न आया होता। उन्होंने कहा था कि कोलकाता की
जो सरलता है‚ वह कठिन है। वह भी चोट करता है।
फिर साल दो साल बाद आना हुआ उनका कोलकाता में। इस बीच
दिल्ली आने को तो कहा था उन्होंने मगर अपनी जिंन्दगी ऐसी
रही कि कोई कार्य योजनाबद्ध ढंग से हो नहीं पाया। वे
कोलकाता आए तो निराला पर तीन दिवसीय आयोजन था। नामवर जी से
लेकर तमाम देश के रचनाकार यहाँ उपस्थित थे। वहीं सभा के
बीच–बीच में होने वाले अंतरालों में मुलाकात व बात होती
रही। डॉक्टर सुकीर्ति गुप्ता से मैंने पेशकश रखी कि क्यों
न आपके आवास पर टालीगंज में एक बैठक हो ले। केदार जी की
कविताएँ सुनी जाएँ। सुकीर्ति जी राजी हो गईं।
केदार जी पहले तो मान ही नहीं रहे थे‚ पर मुझसे इनकार करते
न बना उनसे। वे बड़े थे पर मेरा प्रस्ताव भी शायद उन्हें कम
आत्मीय न लगा हो। उनके राजी होने के बाद तो मैंने समारोह
में आए विष्णु खरे जी को भी राजी कर लिया। सुकीर्ति जी को
इसकी भी जानकारी दे दी कि कोलकाता के कुछ रचनाकार व केदार
जी तथा खरे जी आपके आवास पर बैठेंगे‚ इधर का नया लिखा
सुना-सुनाया जाएगा। वे राजी हो गईं। अगले दिन समाचार
पत्रों में इसकी एक खबर भी दे थी। बैठक दूसरे ही दिन होनी
थी। मगर कार्यक्रम वाले दिन सुकीर्ति जी का पारा गरम पाया।
यह क्या किया। सूचना अखबार में क्यों दे दी। सुबह से फोन आ
रहे हैं तमाम लेखकों के कि सुकीर्ति जी आपने हमें नहीं
बुलाया‚ अपने घर की गोष्ठी में। मैं उस समय संसार का सबसे
मूर्ख और दुखी जीव था। केदार जी कैसे कहूँ? बड़ी मुश्किल से
तो राजी किया था। पर सुकीर्ति जी मुझे पीटने पर उतारू थीं।
सभी के सामने लताड़ना शुरू कर चुकी थीं। सेमिनार भारतीय
भाषा परिषद में था‚ वहीं। खैर। मना किया। विष्णु जी को भी
केदार जी को भी। वे तो खुश ही हुए कि अपने ढंग से वे
कोलकाताकी शाम गुजारेंगे। मेरे कहने से वे बँध गए थे। वे
चाहते तो दिखावे के लिए ही सही‚ बुरा मान सकते थे। मगर वे
मीठी मुस्कान के साथ मेरी बेवकूफियों के साक्षी भर रहे।
सुकीर्ति जी की किसी बात का मैं बुरा मान ही नहीं सकता था।
वे मेरी गुरू इला जी को पढ़ा चुकी थीं। और वे लगातार अपने
व्यवहार से मुझे इस बात का एहसास दिलाती रहती हैं कि मैं
उनका अपना हूँ। बहुत अपना। प्रतिभा को लोगों ने गलत फहमी
से उनकी बेटी समझ लिया था। तो बेहद खुश हुई थीं।
अस्तु 'धु्रवदेव मिश्र पाषाण’ की एक पुस्तक का लोकार्पण
उन्होंने किया था। इस अवसर पर उनके मुँह से पहली बार उनकी
यादगार कविता 'माझी का पुल’ मैंने सुनी थी। जानकर अचरज ही
हुआ कि वह कविता भी उन्हें याद नहीं थी। मगर काव्य–पाठ का
अंदाज मोहक। बातें तह तक पहुँच कर ही करते हैं। आधुनिकता
और परंपरा दोनों की लगाम बराबर वे साधे रहते हैं। वे
कोलकाता आते रहे और मुलाकातें होती रहीं। मगर जो नहीं हो
सका तो उन पर किया गया शोध। दो एक बार उन्होंने कहा भी कि
थीसिस लेकर दिल्ली चले आओ। इसका कुछ करते हैं। किसी
प्रकाशक को ही दे दो। पत्रकार कृपाशंकर चौबे बता रहे थे–
किताबघर वाले केदार जी पर किए आपके काम के बारे में पूछ
रहे थे। मन ऐसा उचटा रहा कि फिर जल्द नया गाइड तय नहीं कर
सका।
डॉ शंभुनाथ ने केदार जी के सामने कहा कि इनका शोध मेरे
निर्देशन में फिर हो जाएगा। मगर जब मैं उनसे मिला तो वे
शोधकार्य को वह दिशा देने लगे जिससे मैं कतई सहमत नहीं था।
मुझे अपने सोचे –समझे और जाने हुए को ही करना है। उसे जो
लिखा जा चुका है। हाँ उनके नए लिखे पर फिर कुछ जोड़ना है पर
उसकी दिशा नहीं बदलनी। पीएचडी नहीं मिलनी है तो न मिले। जब
मैं अमृतसर में पहुँचा तो कुछ दिनों बाद ललक जगी कि
गुरूनानक देव विश्वविदयालय से ही इस काम पर पीएचडी कर ली
जाए। गाइड तय कर लिया। मन माफिक लगे। फार्म भी ले आया। नए
सिरे विश्वविदयालय के हिसाब से सिनाप्सिस तैयार की। मगर
एकाएक जालंधर तबादला हो गया। और फिर वह हसरत अधूरी रह गई।
मगर केदार जी मेरे जीवन में केवल काव्य के विषय ही नहीं रह
गए थे। उन्होंने रचने व जीने की दृष्टि मुझे चुपचाप दी।
जीवन की प्राथमिकताएँ चुनने में उनकी रचनाओं ने भी रास्ता
दिखाया। केदार जी पर मैंने एक कविता ही लिख डाली थी–
'नामवर को बार-बार तुम्हें त्रिलोचन और मुझे तुम क्यों
लगते हो अच्छे केदारनाथ सिंह? शायद इसलिए कि स्वाद एक गंध
का नाम है् गंध एक स्मृति है जो बहती है हमारी धमनियों में
जिसमें नाव की तरह तिरता है एक प्रकाश स्तंभ जो जीवंत
इतिहास है। सोचता हूँ तुम्हारी कविताएँ नहीं होतीं तो मैं
क्या पढ़ता शब्द परिचय के बावजूद? और तुम क्या लिखते? स्वयं
तुम्हारी कविता ही माझी का पुल है् मल्लाह के खुश होने की
परछाई।’
त्रिलोचन जी ने एक बार मुलाकात में मुझे बताया था कि केदार
जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह जिस बात को कहना चाहते
हैं उन्हें इस खूबी के साथ छिपा देते हैं कि उसका आभास भर
होता है पर मूल वक्तव्य खोजते रह जाएँगे। सचमुच केदार के
अंदर की विलक्षणता को तलाश करने के लिए जिस व्यापक दृष्टि
की जरूरत है‚ वह अर्जित करनी पड़ती है। यों ही कोई युवा
पीढ़ी की रचना का नायक नहीं हो जाता। और दुरूहता के बावजूद
लोकप्रिय। देहाती के बावजूद आधुनिकतम।
इधर दिल्ली से आईएएस और संस्कृति विभाग में डिप्टी
सेक्रेटरी कवि–चित्रकार शिवनारायण सिंह 'अनिवेद’ ने ई मेल
पर बताया कि केदार जी मुझे अब भी याद करते हैं‚ तो सुखद
लगा।
१६ दिसंबर
२००२ |